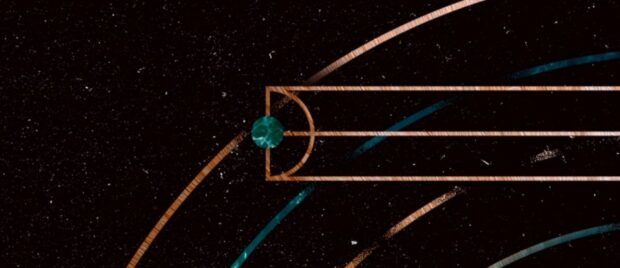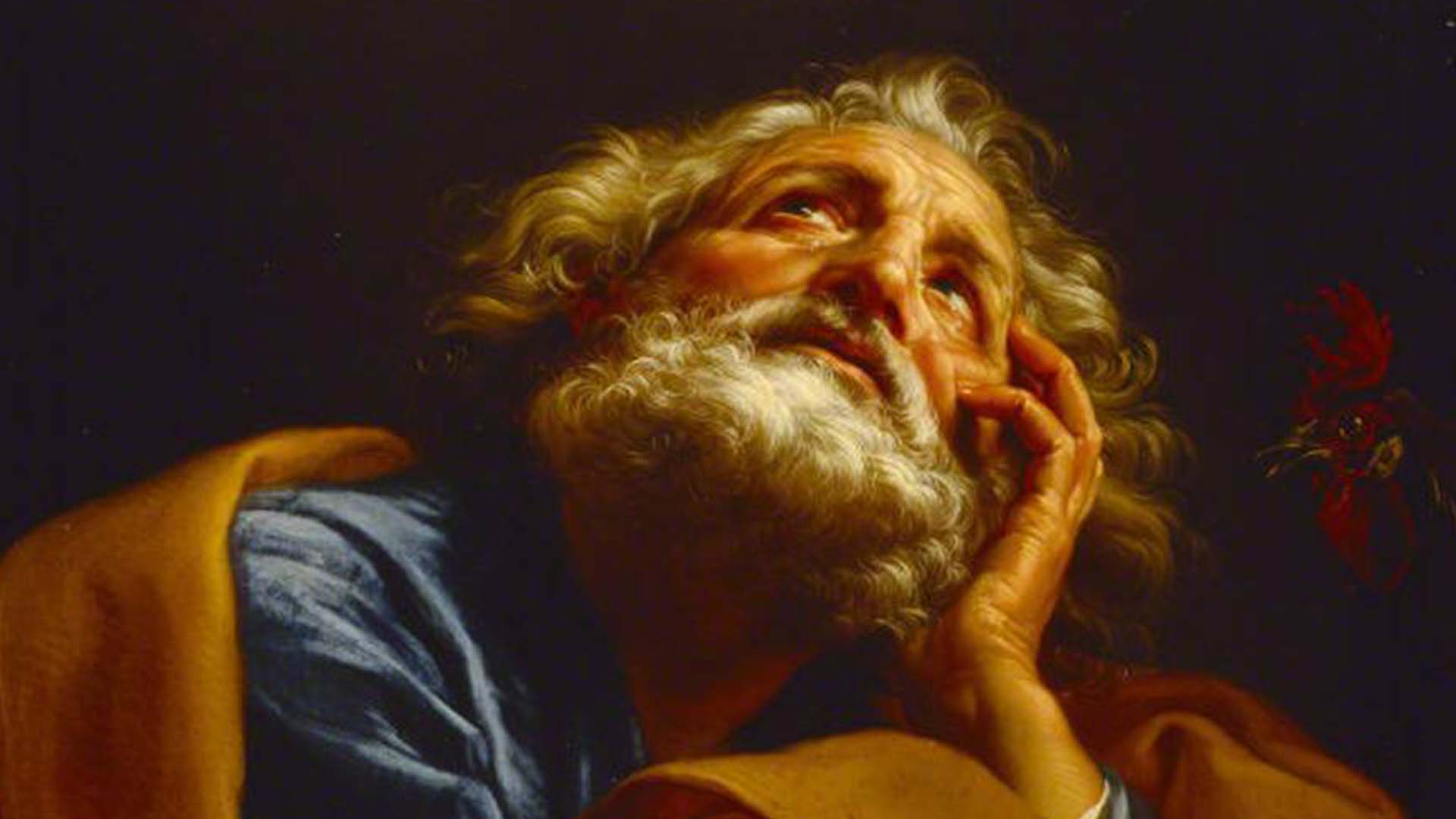
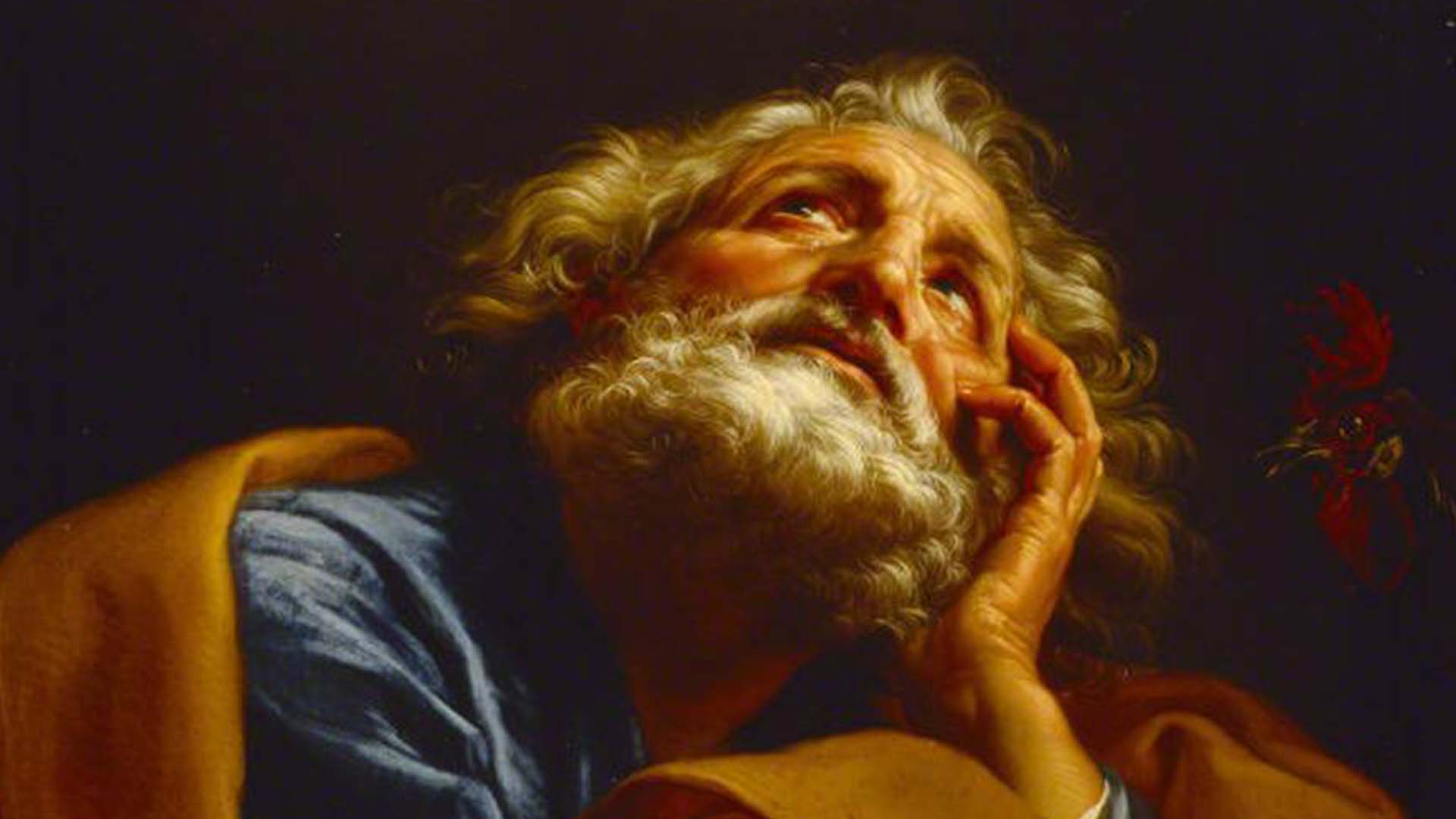
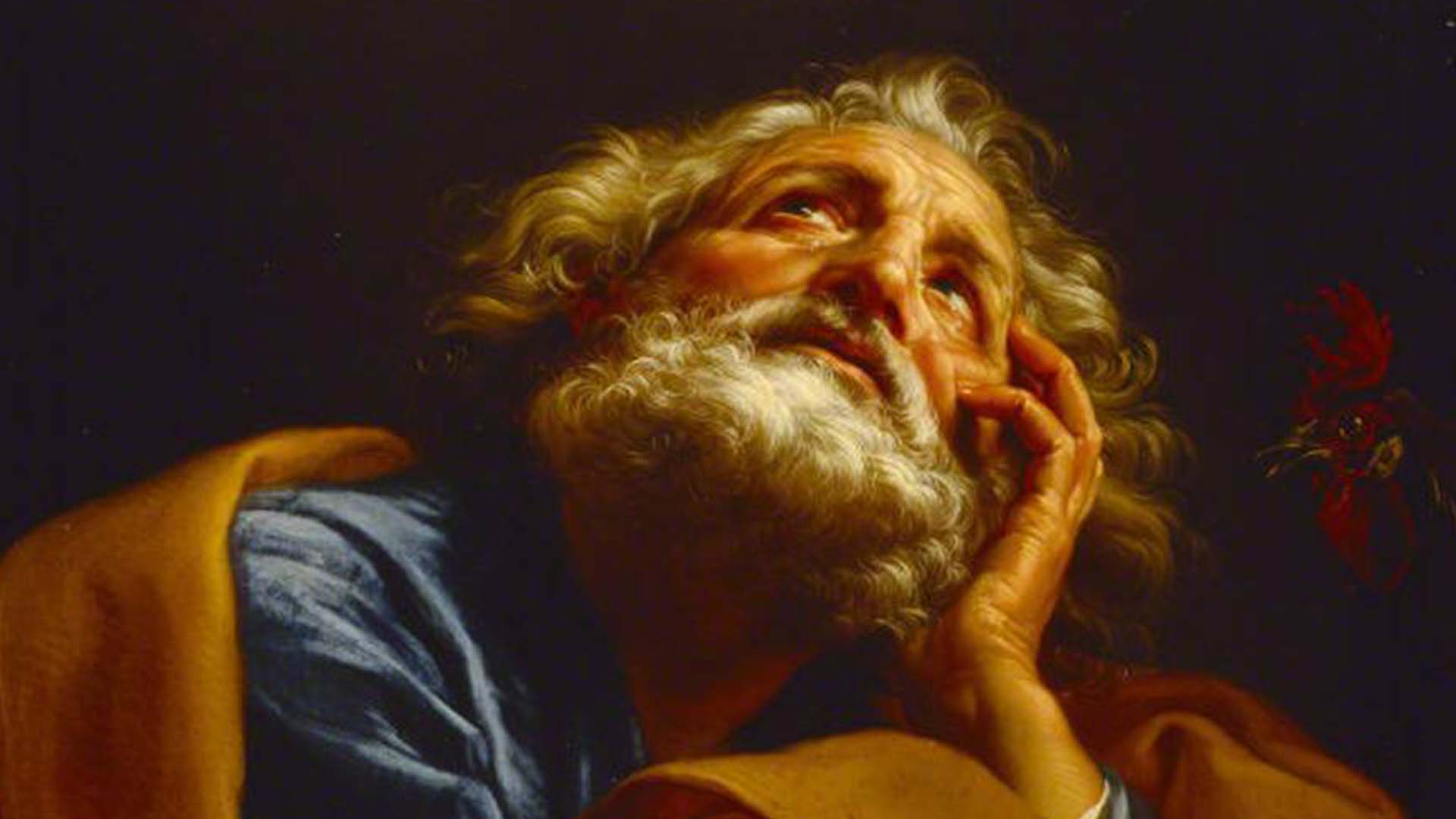
(सम्पूर्ण) सत्य में एक
11 अगस्त 2022


पौलुस में अनुग्रह
18 अगस्त 2022पवित्रशास्त्र को जानना


सम्पादक की टिप्पणी: यह टेबलटॉक पत्रिका श्रंखला का दूसरा अध्याय है: नए नियम की पत्रियाँ
प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि बाइबल पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि लोग इसके द्वारा जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। यह आरोप सही होगा यदि बाइबल परमेश्वर का वस्तुनिष्ठ वचन नहीं होता, यदि यह केवल एक लचीली वस्तु के समान होता, जो किसी के स्वयं के उपदेशों को सिखाने के लिए आकार देने, तोड़-मरोड़ करने, और विकृत करने में सक्षम होता। यह आरोप तब सही होगा यदि पवित्रशास्त्र में जो नहीं है उसे पढ़ना परमेश्वर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अपराध नहीं है। यद्यपि, यह विचार कि बाइबल हमारी इच्छा के अनुसार कुछ भी सिखा सकती है तब सही नहीं है यदि हम नम्रतापूर्वक पवित्रशास्त्र के पास जाते हैं यह सुनने के प्रयास में कि बाइबल स्वयं के विषय में क्या कहती है।
कभी-कभी विधिवत ईश्वरविज्ञान (systematic theology) को अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि इसे पवित्रशास्त्र पर एक दार्शनिक प्रणाली के अनुचित आरोपण के रूप में देखा जाता है। इसे एक पूर्वावधारित प्रणाली (preconceived system) के रूप में देखा जाता है, एक ऐसे बिस्तर के समान जिसमें पवित्रशास्त्र को सही बैठाने के लिए इसके अंगों और उपांगों को काटने के लिए बाध्य किया जाता है। यद्यपि, विधिवत ईश्वरविज्ञान के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि स्वयं बाइबल में एक सत्य की प्रणाली समाविष्ट है, और यह ईश्वरविज्ञानी का कार्य है कि प्रणाली को बाइबल पर न थोपे, अपितु उस प्रणाली को समझ कर जिसे बाइबल सिखाती है एक ईश्वरविज्ञान का निर्माण करे।
धर्मसुधार के समय, पवित्रशास्त्र के अनियन्त्रित, अव्यवहार्य, और काल्पनिक अर्थानुवादों को रोकने के लिए, धर्मसुधारकों ने एक मूल सिद्धान्त को निर्धारित किया जो सभी बाइबलीय अर्थानुवादों को संचालित शासित करता था। यह विश्वास का उपमान (analogy of faith) कहा जाता है, जिसका मूलतः अर्थ है कि पवित्रशास्त्र अपने स्वयं का अर्थानुवादक है। अन्य शब्दों में, हमें पवित्रशास्त्र को पवित्रशास्त्र के अनुसार अर्थानुवादित करना है। अर्थात्, बाइबल की सम्पूर्ण शिक्षा पवित्रशास्त्र में किसी एक विशेष पद के अर्थ के अनुवाद में सर्वोच्च विवाचक (supreme arbiter) है।
विश्वास के उपमान के सिद्धान्त (principle) के पीछे पहले से यह निश्चयतता है कि बाइबल परमेश्वर का प्रेरित वचन है। यदि यह परमेश्वर का वचन है, तो इसलिए इसे समनुरूप और सुसंगत होना चाहिए। यद्यपि, निन्दकों का कहना है कि समनुरूपता छोटे मस्तिष्कों के लिए डराने की कोई वस्तु है। यदि ऐसा सत्य होता, तो हमें कहना पड़ता कि सभी मस्तिष्कों में से सबसे छोटा मस्तिष्क परमेश्वर का है। परन्तु समनुरूपता में सहज रूप से छोटा या निर्बल कुछ भी नहीं पाया जाता है। यदि यह परमेश्वर का वचन है, तो कोई व्यक्ति उचित रूप से सम्पूर्ण बाइबल के सुसंगत, सुबोध, और एकीकृत होने की अपेक्षा कर सकता है। हमारी धारणा है कि परमेश्वर अपनी सर्वज्ञता के कारण, स्वयं का विरोध करने के लिए कभी दोषी नहीं होगा। इसलिए किसी विशेष खण्ड के एक अर्थानुवाद का चुनाव करना पवित्र आत्मा के प्रति निन्दक है जो अनावश्यक रूप से खण्ड को उस खण्ड के साथ द्वन्द्व में ले आता है जिसे उसने कहीं और प्रकट किया है। इसलिए धर्मसुधारक व्याख्याशास्त्र या अर्थानुवाद का शासित सिद्धान्त विश्वास का उपमान है।
एक दूसरा सिद्धान्त जो पवित्रशास्र के वस्तुनिष्ठ अर्थानुवाद को शासित करता है वह यथार्थ अर्थ (सेन्सस लिटरैलिस – sensus literalis) कहलाता है। कई बार लोगों ने मुझसे सन्देह करते हुए कह चुके हैं, “आप बाइबल का शाब्दिक अनुवाद तो नहीं करते हैं?” मैं कभी भी “हाँ” कह कर प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूँ, न ही मैं कभी “न” कहकर प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मैं सदैव यह कहकर प्रश्न का उत्तर देता हूँ, “निस्सन्देह, बाइबल का अर्थानुवाद करने का अन्य कौन सा उपाय है?” यथार्थ अर्थ से तात्पर्य यह नहीं है कि पवित्रशास्त्र में हर एक स्थल का “भावशून्य अर्थ” (woodenly literal) अनुवाद दिया गया है, परन्तु यह है कि हमें बाइबल का उसी भाव में अर्थानुवाद करना चाहिए जिस भाव में वह लिखी गयी है। दृष्टान्तों का अर्थानुवाद दृष्टान्तों के रूप में किया गया है, संकेतों का संकेतों के रूप में, कविता का कविता के रूप में, शिक्षात्मक साहित्य का शिक्षात्मक साहित्य के रूप में, ऐतिहासिक वृतान्त का ऐतिहासिक वृतान्त के रूप में, असाम्यिक पत्रियों का आसम्यिक पत्रियों के रूप में। शाब्दिक अर्थानुवाद का वह सिद्धान्त वही सिद्धान्त है जिसका उपयोग हम किसी भी लिखित स्रोत का विश्वसनीय ढंग से अर्थानुवाद करने के लिए करते हैं।
शाब्दिक अर्थानुवाद का सिद्धान्त हमें एक और नियम देता है, अर्थात् बाइबल को एक भाव में किसी अन्य पुस्तक के समान पढ़ना। यद्यपि बाइबल अन्य पुस्तक के समान नहीं है क्योंकि इसमें ईश्वरीय प्रेरणा का अधिकार है, तथापि, लिखित स्थल पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा क्रियाओं को संज्ञाओं में और संज्ञाओं को क्रियाओं में नहीं परिवर्तित कर देती है। केवल इसलिए क्योंकि यह ईश्वरीय रूप से प्रेरित है कोई भी विशेष, गोपनीय, रहस्यपूर्ण, गूढ़ अर्थ किसी भी स्थल पर नहीं उड़ेल दिया गया है। न ही ऐसी कोई रहस्यवादी योग्यता है जिसे हम “पवित्र आत्मा की यूनानी भाषा” (Holy Ghost Greek) कहते हैं। नहीं, बाइबल को भाषा के सामान्य नियमों के अनुसार अर्थानुवाद किया जाना चाहिए।
इस बिन्दु का निकटतम सिद्धान्त यह है कि जो स्पष्टता से व्यक्त है उसका अर्थानुवाद जो अव्यक्त है उसके द्वारा किए जाने के स्थान पर, जो अव्यक्त है उसका अर्थानुवाद जो स्पष्टता से व्यक्त है उसके साथ किया जाना चाहिए। अर्थानुवाद के इस विशिष्ट नियम का निरन्तर उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए, हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि “जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परन्तु अनन्त जीवन पाए,” और हम में से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्यूंकि बाइबल यह सिखाती है कि जो कोई विश्वास करेगा वह बचाया जाएगा, इसलिए इसका यह तात्पर्य है कि कोई भी, पवित्र आत्मा के पूर्व पुनरुज्जीवित कार्य के बिना, विश्वास का अभ्यास कर सकता है। अर्थात्, क्यूंकि विश्वास करने की बुलाहट सबको दी गयी है, तो इसका तात्पर्य यह है कि सबके पास बुलाहट को पूरा करने की स्वाभाविक योग्यता है। फिर भी उसी सुसमाचार के लेखक ने तीन अध्ययों के पश्चात यीशु को हमें यह समझाते हुए बताया है कि कोई भी यीशु के पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि वह पिता की ओर से नहीं दिया गया हो (6:65)। अर्थात्, ख्रीष्ट के पास आने की हमारी नैतिक योग्यता को स्पष्ट रूप और विशिष्ट रूप से परमेश्वर के सम्प्रभु अनुग्रह से पृथक होने के लिए शिक्षित किया गया है। इसलिए, सभी निहितार्थ जो कि भिन्न सुझाव देते हैं उन्हें स्पष्ट शिक्षा को स्थल से निकाले गए उन निहितार्थों के अनरूप बनाने पर बल देने के स्थान पर स्पष्ट शिक्षा के अन्तर्गत सम्मिलित होने चाहिए।
अन्त में, अस्पष्ट खण्डों का अर्थानुवाद उन खण्डों के द्वारा करना सदैव महत्वपूर्ण होता है जो कि स्पष्ट हैं। यद्यपि हम पवित्रशास्त्र की आधारभूत स्पष्टता की पुष्टि करते हैं, उसी समय हम में यह नहीं कहते कि सभी खण्ड समान रूप से स्पष्ट हैं। अनगिनत विधर्मता तब विकसित हुई जब लोगों ने खण्डों को स्पष्ट करने के स्थान पर अस्पष्ट खण्डों की अनुरूपता पर बल दिया, जिसने पवित्रशास्त्र के पूरे सन्देश को विकृत कर दिया है। यदि पवित्रशास्त्र के एक भाग में कुछ अस्पष्ट है, तो वह सम्भवतः पवित्रशास्त्र में कहीं और स्पष्ट किया गया है। जब हमारे पास पवित्रशास्त्र में दो खण्ड होते हैं जिनका हम विभिन्न प्रकार से अर्थानुवाद कर सकते हैं, तो हम बाइबल का अर्थानुवाद सदैव इस प्रकार से करना चाहते हैं जिससे पवित्रशास्त्र की एकता और अखण्डता के मूल सिद्धान्त का उल्लंघन न हो।
ये बाइबलीय अर्थानुवाद के कुछ मूलभूत, व्यावहारिक सिद्धान्त हैं जिन्हें मैंने वर्षों पूर्व अपनी पुस्तक नोइंग स्क्रिपचर (Knowing Scripture) में बताए हैं। मैं उस पुस्तक की बाक यहाँ इसलिए करता हूँ क्योंकि कई लोगों ने मुझसे यह व्यक्त किया कि बाइबलीय अर्थानुवाद के एक विश्वसनीय अभ्यास में उनके मार्गदर्शन में यह कितनी सहायक रही है। अर्थानुवाद के सिद्धान्तों को सीखना हमारे स्वयं के अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए अत्याधिक सहायक है।
यह लेख मूलतः टेबलटॉक पत्रिका में प्रकाशित किया गया